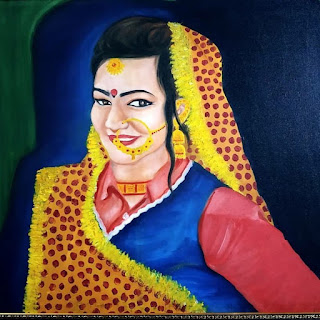उत्तराखंड में अधिकतर भागो में कड़ाके की ठंड
पड़ती है और सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी ढल जाता है। राते लम्बी होती है। एक वह दौर था , जब टीवी और मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ
करते थे। उस समय रात को बड़े बूढ़े या ईजा आण- काथ सुनाकर समय व्यतीत करती थी। एक कहानी मैंने भी बचपन में बहुत सुनी थी -
" चल तुमड़ी बाट बाट , मैके जाणु बुड़ीय बात "
पहलियों को आण कहा जाता था जैसे " भम बुकि
, माट मी लुकी " का उत्तर - मूली होता था।
घर के छोटे , नौजवान और बुजुर्ग अंगीठी में कोयला जलाकर एक जगह आग तापते थे
और फिर मूंगफली या भुने भट्ट खाये जाते थे और फिर शुरू होता था - आण- काथ का दौर। परिवार के बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते थे , खूब
हंसी ख़ुशी का दौर चलता था। सबसे बड़ी बात वो
आग की अँगीठी या सँगेड़ी सारे परिवार को एकजुट कर देती थी। सब गिले - शिकवे उसी अँगीठी के इर्द गिर्द सुलझ
जाते थे।
बाँज के लकड़ियों के कोयले बहुत देर तक गर्मी
देते थे और चीड़ के फल जिसे " ठीठे " कहा जाता था , बड़ी जल्दी राख हो जाते
थे। वो दौर ऐसा था , जिसमे सबके लिए एक दूसरे के लिए समय होता था।
अब शायद
"आण- काथ " की जगह टीवी और मोबाइल ने ले लिया है और अँगीठी जलनी अब
बंद सी हो गयी है और परिवार वालो के पास भी अब वक्त थोड़ा कम हो चला है। कुछ परम्पराएं हमेशा जीवित रहनी चाहिए और शायद ये
परम्परा उन्ही में से एक थी।